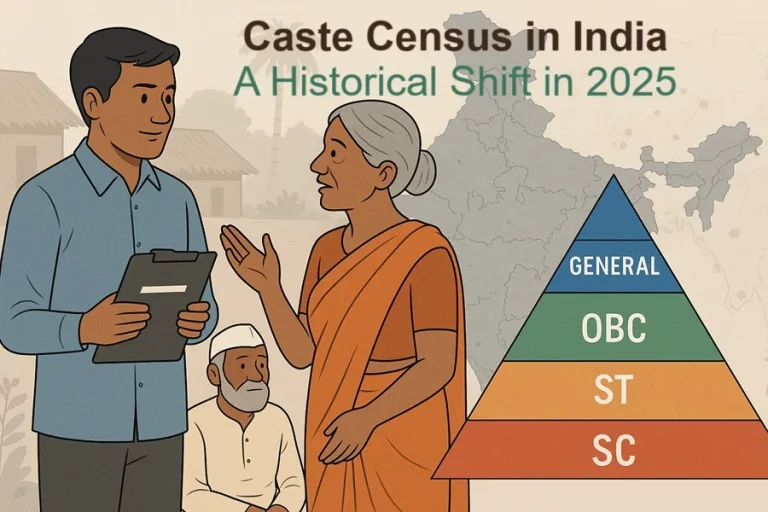इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने भारत की अगली जनसंख्या जनगणना को अधिसूचित किया, जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी: 1931 की जनगणना के बाद पहली बार जाति-आधारित डेटा एकत्र किया जाएगा। जातियों की इस गणना के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होंगे। यह तथ्य कि इसे आयोजित किया जा रहा है, भारत के राजनीतिक माहौल और राज्य अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को कैसे देखता है, के बारे में बहुत कुछ बताता है।
पूरे इतिहास में, डेटा संग्रह वह साधन रहा है जिसके द्वारा शासक उन लोगों को समझते थे जिन पर वे शासन करते थे। लेकिन जनगणना के तरीके, गहराई और उद्देश्य सदियों से विकसित हुए हैं: चोल जैसे मध्ययुगीन साम्राज्यों के तहत गठबंधन बनाने से लेकर मुगलों, राजपूतों और मराठों के तहत जाति और आर्थिक गतिशीलता को संतुलित करने तक, ब्रिटिश राज के तहत नस्लवादी नृवंशविज्ञान और वैचारिक नियंत्रण तक।
पुस्तक 2, अध्याय 35 में, पाठ के लेखकों ने राजस्व अधिकारियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया, जिन्हें खेती की गई भूमि, छूट और अनुदानों को रिकॉर्ड करना था, और “चार सामाजिक वर्गों” के घरों को सूचीबद्ध करना था। बेशक, ऐसे डेटा की गुणवत्ता को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए गुप्त एजेंटों को सभी सूचनाओं को सत्यापित करना था। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य को न केवल उद्योग और कृषि से राजस्व प्राप्त होता था, बल्कि अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने से भी राजस्व प्राप्त होता था। पुस्तक 3 में, ब्राह्मणवादी ग्रंथों द्वारा परिकल्पित सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखते हुए जाति के अनुसार जुर्माना और दंड सूचीबद्ध किए गए थे।
हमें नहीं पता कि शुरुआती भारतीय राज्यों ने वास्तव में अर्थशास्त्र को किस हद तक लागू किया था, लेकिन शुरुआती शताब्दियों के शिलालेखों से पता चलता है कि शासक जातियों पर नज़र रखना चाहते थे। गंगा के मैदानों में बैंकर, व्यापारी, बुनकर, मुंशी और कारीगर जैसे समूह जाति-जैसे सामूहिक बना रहे थे और शहर के प्रशासन में भाग ले रहे थे। जैसा कि इतिहासकार चित्ररेखा गुप्ता ने ‘प्राचीन भारत के लेखकों की कक्षा’ में लिखा है, ऐसे समूह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक शक्ति थे। मध्यकाल के दौरान, लगभग 600 और 1100 ई. के बीच, वे पूरे उपमहाद्वीप में विकसित हुए। राज्यों को नगर सभाओं, ग्राम सभाओं, व्यावसायिक सभाओं और जाति सभाओं से निपटना पड़ता था – सभी के अपने कानून, परंपराएँ और अधिकारों के दावे थे।
चोल साम्राज्य, जो आरंभिक मध्ययुगीन राज्य था, ने कर की दरें तय करने के लिए कई भूमि सर्वेक्षणों का आदेश दिया, लेकिन कभी-कभी किसानों और भूस्वामियों की संगठित सभाओं से विरोध का सामना करना पड़ा। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब साम्राज्य अपने चरम पर था, तो यह बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। वास्तव में, भूमि सर्वेक्षणों ने चोलों को मंदिरों के दान को रिकॉर्ड करके और बनाए रखकर समुदायों के साथ गठबंधन बनाने में मदद की। लेकिन 11वीं शताब्दी के अंत तक, जब विजय की लहर धीमी हो गई और दरबार कमजोर हो गया, तो शिलालेखों से पता चलता है कि चित्तिरमेली-पेरियानाडु गठबंधन जैसी “सुपर असेंबली” – जिसमें किसान, जमींदार और ब्राह्मण शामिल थे – ने राज्य को कितना राजस्व देना है, इस पर अपने स्वयं के निर्णय लेने शुरू कर दिए। 1300 के दशक तक, ऐसे गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक पदानुक्रमों पर अधिकार जता रहे थे और अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए पैरवी कर रहे थे। किसी भी मध्ययुगीन भारतीय शासक के लिए, भूमि को मापना और जाति की निगरानी करना बिल्कुल आवश्यक था।
मुगल, मराठा और जातिगत आंकड़ों की सीमाएँ
जबकि शुरुआती मध्ययुगीन काल से कुछ राजस्व रिकॉर्ड बचे हुए हैं, 1500 के दशक से तस्वीर में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जैसे नए बारूदी राज्यों ने बड़ी नौकरशाही में निवेश किया। हमें दरबारी अबुल फ़ज़ल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी (“अकबर की संस्थाएँ”) से मुगल प्रशासन की काफी अच्छी तस्वीर मिलती है। उन्होंने जिलों से अनुमानित राजस्व दर्ज किया, जो जाहिर तौर पर स्थानीय नौकरशाहों द्वारा किए गए मापों पर आधारित था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उत्तर भारत की कई जातियों पर भी ध्यान दिया, जिसमें ठाकुर, राजपूत, जाट और अन्य ज़मींदार समुदायों का उल्लेख किया गया।
हालाँकि, मुगल नौकरशाही ने आँकड़ों का पहाड़ खड़ा किया, लेकिन डेटा की गुणवत्ता बेहद संदिग्ध थी। ‘मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर पुनर्विचार’ में, इतिहासकार सुमित गुहा ने मुगल राजस्व दस्तावेजों की आलोचनात्मक जाँच की। उन्होंने पाया कि कर राजस्व का मूल्यांकन अक्सर अपडेट नहीं किया जाता था: आखिरकार, फसलों का सटीक अनुमान लगाने के लिए नौकरशाहों को मौसम और वर्षों के अनुसार गांवों का दौरा करना पड़ता – ऐसा कुछ जिसके लिए उनके पास संसाधन या इच्छाशक्ति नहीं थी। अकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर ने अपने संस्मरणों में आय-ए-अकबरी में दिए गए राजस्व के समान ही आँकड़े उद्धृत किए थे – जो तब तक 20-30 साल पुराने हो चुके थे।
मुगल नौकरशाहों ने राजनीतिक दावे करने के लिए अशांत या अविजित प्रांतों के लिए राजस्व अनुमान भी गढ़े। जहाँ उनका नियंत्रण था, वहाँ उन्होंने फसल का एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा जबरन मांगा। बियॉन्ड कास्ट: आइडेंटिटी एंड पावर इन साउथ एशिया में गुहा ने यह भी बताया है कि कुछ जातिगत डेटा गाँव के स्तर पर दर्ज किए गए थे, ताकि जाति के मुखियाओं से राजस्व की माँग की जा सके। आश्चर्य की बात नहीं है कि गाँव के मुंशी अक्सर करों से बचने के लिए संख्याओं में हेराफेरी करते थे; स्थानीय ज़मींदार अधिकारियों को रिश्वत देते थे; और अधिकारी सक्षम दिखने के लिए डेटा गढ़ते थे। अगर इंस्पेक्टरों द्वारा पकड़े जाते, तो क्रूर दंड दिया जाता था। लेकिन चूँकि मुगल अधिकारियों के पास पहले से ही सटीक राजस्व अनुमान नहीं थे, इसलिए वे कभी-कभी मुंशियों, कलेक्टरों और गाँव के मुखियाओं को कोड़े मारते या कैद कर लेते थे, जो उचित कारणों से उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते थे। गुहा लिखते हैं: “…न केवल भ्रष्ट अधिकारी बल्कि व्यापारी, बैंकर और वास्तव में, भुखमरी से बचने के लिए प्रयासरत छोटे किसानों के पास भी जानकारी छिपाने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन था… [डेटा] किसानों, स्थानीय प्रमुखों और अधिकारियों के बीच निरंतर संघर्ष से उत्पन्न होते थे… परिणाम में अलिखित रिश्वत की बाढ़ और दर्ज [गलत] आँकड़ों का खजाना था।” भ्रष्टाचार राज्य के हर स्तर पर समाहित हो गया; यूरोपीय यात्री अक्सर मुगल अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत के बारे में शिकायत करते थे।
नैंसी के सर्वेक्षण, एक खानसुमारी, ने हर जिले की राजधानी में जाति के आधार पर घरों की गणना की: शायद भारत में पहली सच्ची ‘जाति जनगणना’। राजस्थान के अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की खानसुमारी और गांव के सर्वेक्षण किए जिन्हें याददस्ती कहा जाता है; लेकिन ग्रामीण और शहरी डेटा को एकत्र करने की अवधारणा विकसित नहीं हुई। नैंसी ने अपनी सूची में अपने ओसवाल समुदाय को प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि प्रत्येक इलाके में अलग-अलग जाति पदानुक्रम थे। न ही वह धर्म को लेकर बहुत अधिक चिंतित थे। हालाँकि, यह जल्द ही बदलने वाला था।
ब्रिटिशों का अधिग्रहण – औपनिवेशिक जाति सर्वेक्षण
गुहा (बियॉन्ड कास्ट) लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक, कई भारतीय राज्यों-विशेष रूप से मराठा प्रभुत्वों में-काफ़ी विस्तृत जाति गणना (घरों के अनुसार) विकसित हो चुकी थी, जिसका उपयोग सामाजिक पदानुक्रमों को विनियमित करने और विभेदक कराधान और विशेषाधिकार लागू करने के लिए किया जाता था। आबादी अपेक्षाकृत गतिशील बनी रही, जो प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया करती थी। इस विस्मयकारी जटिल प्रणाली में अंग्रेज़ आए, जिनके पास भारतीय समाज के कामकाज के बारे में अपने स्वयं के (अधिकांशतः काल्पनिक) विचार थे, साथ ही राजस्व के प्रति एक कठोर दृष्टिकोण भी था।
स्थानीय रूप से रिपोर्ट किए गए डेटा पर कुछ हद तक उचित रूप से संदेह करने वाले अंग्रेजों ने अपने स्वयं के सर्वेक्षण करने के लिए वेतनभोगी अधिकारियों को भेजा। गुहा लिखते हैं कि भारतीय राज्यों के विपरीत, अंग्रेजों ने घरों की नहीं, बल्कि व्यक्तियों की गिनती की। उन्होंने स्थायी पते और सीमाओं पर भी ज़ोर दिया, क्योंकि उन्हें प्रवासन पर संदेह था। इसने बंजारा जैसे घुमंतू व्यापारियों के साथ-साथ पशुपालक समुदायों को तबाह कर दिया। संभवतः सबसे अधिक नुकसानदायक बात यह रही कि अंग्रेजों ने भारत की बदलती पहचानों पर अपनी श्रेणियां और राजनीतिक आवश्यकताएं थोप दीं।
1845-46 में, वन जनजातियों के विद्रोहियों से लड़ने के बाद, बॉम्बे सरकार ने जाति के बजाय धर्म के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करने और “जंगली जनजातियों” की अलग से पहचान करने पर जोर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेज़ धार्मिक वर्गीकरण के प्रति और भी अधिक जुनूनी हो गए। रानी विक्टोरिया की इस घोषणा के बाद कि राज भारतीय रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अंग्रेजों ने उन रीति-रिवाजों को परिभाषित करने के लिए उच्च-जाति के भारतीय अभिजात वर्ग-मुख्य रूप से ब्राह्मणों से परामर्श किया। परिणाम बहुत ही पक्षपातपूर्ण थे।
जैसा कि इतिहासकार निकोलस डर्क्स ने कास्ट्स ऑफ़ माइंड: कोलोनियलिज़्म एंड द मेकिंग ऑफ़ मॉडर्न इंडिया में उल्लेख किया है, एचएच रिस्ले, जिन्होंने 1901 की बंगाल जनगणना की देखरेख की थी, ने मनुस्मृति जैसे शास्त्रों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसका अधिकांश जातियाँ वास्तव में पालन नहीं करती थीं। रिस्ले ने जाति को ‘आर्यन’ वंश से जोड़ने वाले नस्लीय सिद्धांतों को भी पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के निषेध जैसे उच्च-जाति के मानदंडों का समर्थन किया, जिनके खिलाफ हिंदू सुधारक लड़ रहे थे। उन्होंने इस नस्लीय हथियारबंद डेटा का इस्तेमाल बंगाल के विभाजन और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग निर्वाचिकाओं की मांग करने के लिए किया।
भारतीय अभिजात वर्ग ने इन ब्रिटिश श्रेणियों को जल्दी से अपना लिया, क्योंकि वे उस समय के मानकों के अनुसार ‘वैज्ञानिक’ प्रतीत होते थे। भारत के बारे में औपनिवेशिक सिद्धांत कितने विकृत थे, इस बारे में अभी तक बहुत कम समझ थी। नस्लीय सिद्धांत और द्विआधारी धार्मिक पहचान – हिंदू और मुस्लिम – पूरी तरह से आत्मसात हो गए थे। जाति संगठन पनपे, रेलवे और टेलीग्राफ से जुड़े। हिंदू और मुस्लिम अभिजात वर्ग ने पाया कि धार्मिक आधार पर जाति समूहों के एक बार-विविध बहुरूपदर्शक को समेकित करने से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ। विभाजन की अंतिम मांग एक स्वार्थी औपनिवेशिक साम्राज्य द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर आधारित पहचान निर्माण के दशकों की परिणति थी।
स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय सांख्यिकीविदों और समाजशास्त्रियों की पीढ़ियों ने डेटा संग्रह की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है, जिससे बहुत अधिक मानवीय नीतियां और योजनाएँ बन पाई हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि अच्छे डेटा की गारंटी नहीं है – न ही अच्छे इरादे या अच्छे नीतिगत परिणाम। भारतीय शासकों ने हमेशा माना है कि डेटा शक्ति है।