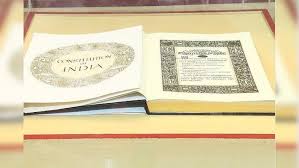नई दिल्ली: ऐसे संकेत हैं कि मौजूदा चार जीएसटी दरों: 5%, 12%, 18% और 28% के अलावा एक नया माल और सेवा कर (जीएसटी) स्लैब पेश किया जाएगा। जीएसटी परिषद में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों, साथ ही वातित पेय पदार्थों के लिए कर दरों को 35% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। लक्जरी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने के भी सुझाव हैं, जैसे 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते और 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियाँ, जिन्हें वर्तमान 18% से 28% जीएसटी के उच्चतम स्लैब में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कपास और कपड़ा वस्तुओं को उनके मौजूदा टैक्स स्लैब से अगले उच्चतम जीएसटी स्लैब दरों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
एक अतिरिक्त जीएसटी स्लैब लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है, खासकर उच्च स्तर पर, जो अप्रत्यक्ष कर संरचना को जटिल बना सकता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान जैसे कई विकसित देशों में एक ही जीएसटी दर है, जो आमतौर पर 5% से 15% के बीच होती है। उच्च बहुस्तरीय जीएसटी स्लैब का अनपेक्षित परिणाम खपत में कमी और व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जीएसटी संग्रह पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है, 2023-2024 में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक, अतिरिक्त 35% टैक्स स्लैब पेश करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, खासकर जब भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही 5.4% की धीमी वृद्धि दर जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।—
संसद में भाषणों में विपक्षी दलों पर इस बात के लिए हमला किया गया कि उन्होंने अतीत या वर्तमान में क्या किया है या क्या नहीं किया है। पिछली नीतियों पर हमला करना आसान है लेकिन उन नीतियों के संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि संविधान में निहित सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाएगा। हालाँकि भारत ने पिछले 75 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि ‘हम, भारत के लोगों’ ने संविधान में निहित वादों को केवल आंशिक रूप से ही पूरा किया है। संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’, ‘स्वतंत्रता’, ‘समानता’ और ‘बंधुत्व’ का वादा किया गया था। ये इसकी बुनियाद हैं. एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में संविधान को बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा सकता है लेकिन ये सिद्धांत बने रहेंगे और आवश्यक परिवर्तनों का मार्गदर्शन करेंगे। यदि इन सिद्धांतों का पालन किया गया होता तो राम राज्य स्थापित हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल गलती से इसे राम मंदिर निर्माण के बराबर बता देता है।
दुर्भाग्य से, कोई भी संविधान की मूल भावना का पालन किए बिना उसके अक्षरों का पालन कर सकता है और समय के साथ, सत्तारूढ़ व्यवस्था ने इसे विकृत करते हुए संवैधानिक रूप से सही होने का दिखावा किया है। उदाहरण के लिए, चुनावों का उद्देश्य लोगों को सत्ता में प्रतिनिधित्व देना है। लेकिन चुनाव जीतना एक कला है. बाहुबल और धनबल का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। मतदाताओं को अक्सर मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है या मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोक दिया जाता है।बहुसंख्यकवाद व्यक्ति की दूसरों के प्रति भाईचारे की भावना और सहानुभूति को कमजोर करता है। सांप्रदायिक विभाजन के बढ़ने से न्याय और भाईचारा कमजोर होता है। जाति और समुदाय के आधार पर लामबंदी भाईचारे को और कमजोर करती है।
अदालतें, जहां लोग न्याय चाहते हैं, तेजी से बहुसंख्यकवादी संवेदनाएं प्रदर्शित कर रही हैं। न्याय में कमजोरों का पक्ष लेना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना शामिल होना चाहिए। हालाँकि, हाशिए पर रहने वाले अधिकांश लोग न्याय के लिए अदालत में जाने और चुपचाप पीड़ा सहने का जोखिम भी नहीं उठा सकते।
नौकरशाही और पुलिस अक्सर मनमाने ढंग से और अल्पसंख्यकों के अहित में कार्य करती हैं। इसने बहुसंख्यक समुदाय को अधिक पक्षपातपूर्ण बनने और यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि इन संस्थानों को उनके हित में काम करना चाहिए। अल्पसंख्यक इसे अपने दूसरे दर्जे के नागरिक बनने के रूप में देखते हैं। इस प्रकार, दोनों समुदायों के बीच न्याय और भाईचारे की भावना खत्म हो गई है। इन सबका सीधा असर लोगों की आज़ादी पर पड़ता है। अल्पसंख्यक न केवल बहुसंख्यकों से डरते हैं बल्कि वे राज्य द्वारा उत्पीड़न के डर में भी रहते हैं। पुलिस द्वारा झूठे मामलों और अदालतों से समय पर न्याय की कमी ने अल्पसंख्यकों में से कई को डरा दिया है। माताएं अपने बच्चों से कहती हैं कि वे सार्वजनिक रूप से अपना मुंह न खोलें। एक उल्लेखनीय उदाहरण में, एक शिक्षिका ने छात्रों से एक कक्षा के साथी को थप्पड़ मारने के लिए कहा और उसे लगा कि उसने जो किया वह उचित था।
संविधान का ‘जीवित वेतन’ का वादा अधूरा है। इसे और बढ़ती असमानता को देखते हुए, जनता का राजनीतिक दलों के दीर्घकालिक वादों पर से भरोसा उठ गया है और वह तुरंत अपने हाथ में कुछ चाहती है। इन्हें प्रधान मंत्री ने ‘रेवड़ी’ (मुफ़्त उपहार) के रूप में वर्णित किया है। ये समानता सुनिश्चित नहीं करते – केवल असमानता में वृद्धि को धीमा करते हैं। जाहिर है, चंद लोगों के हित में काम कर रही सरकार ने संविधान की प्रस्तावना के वादों को तिलांजलि दे दी है। संसदीय बहस सार्थक होती अगर उसने सामूहिक रूप से इन वादों को दोहराया होता और उन्हें पूरा करने के लिए एक लक्ष्य तिथि निर्धारित की होती।
जाहिर है, चंद लोगों के हित में काम कर रही सरकार ने संविधान की प्रस्तावना के वादों को तिलांजलि दे दी है। संसदीय बहस सार्थक होती अगर उसने सामूहिक रूप से इन वादों को दोहराया होता और उन्हें पूरा करने के लिए एक लक्ष्य तिथि निर्धारित की होती।
इन वादों को सुनिश्चित करने का एक तरीका यह होता कि संसद एक प्रस्ताव पारित करती कि नीतियां गांधी के ताबीज – ‘अंतिम व्यक्ति पहले’ – पर आधारित होंगी और पांच वर्षों में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी।
Post Views: 114